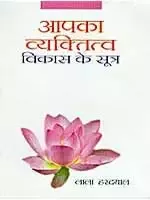|
विविध >> आपका व्यक्तित्व विकास के सूत्र आपका व्यक्तित्व विकास के सूत्रलाला हरदयाल
|
341 पाठक हैं |
||||||
मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त कराने के लिए प्रेरणादायी उपयोगी पुस्तक.....
Aapka Vyaktitva Vikas Ke Sutra
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व की निर्णायक भूमिका होती है। व्यक्तित्व का विकास हम स्वयं भी कर सकते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी और विचारक लाला हरदयाल की इस युगांतकारी अमर कृति में व्यक्तित्व के विकास के सूत्र अत्यन्त सरल और रोचक भाषा-शैली में सुझाए गए हैं। एक अत्यन्त उपयोगी एवं प्रेरणादायी पुस्तक।
(1)
बौद्धिक विकास की आवश्यकता
यह आपका कर्त्तव्य है कि आप अपने मतिष्क की प्रशिक्षित करें, उसका विकास करें, ज्ञान का अधिक से अधिक संचय करें। ज्ञान एक गहरे कूप के समान है, जिसका स्त्रोत अजस्त्र है। आपका मतिष्क एक बाल्टी या गागर के समान है। जितना बड़ा आपका पात्र होगा, उतना ही जल आप कूप से खींच सकेंगे। मन का शारीरिक अंग मष्तिक है। अपने मूल रूप से विकसित होते-होते, मानव-रूप ग्रहण करने पर मानव ने जो दो विशिष्ट वस्तुएँ प्राप्त की हैं, मन उन्हीं में से एक है, और दूसरी वस्तु है-सामाजिक भावना। यह विचित्रतापूर्ण मस्तिष्क, जिसकी प्रत्येक सलवट लाखों वर्षों के क्रमिक विकास की सूचक है, यह वस्तुतः आपको अन्य पशुओं से प्रथक करती है। बहुत से पशुओं में बहुत शक्तिशाली इन्द्रियाँ पायी जाती हैं, चील, चींटी और कुत्ते में मनुष्य की अपेक्षा अधिक चेतना पाई जाती है। किन्तु किसी भी पशु का मानव से अधिक मस्तिष्क नहीं है और न ही उससे ऊँची बुद्धि किसी प्राणी के पास है। यदि आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग उसकी अधिकतम सामर्थ्य के अनुसार नहीं करते, तो आप पशुओं के समान ही हैं।
ज्ञान तथा मानसिक आत्म-संस्कार से आप पर अवर्णनीय वरदानों की वर्षा होगी। इससे आप धर्म और राजनीति के बारे में अन्धविश्वासों और रुढ़ियों के दास नहीं रहेंगे। तब आप अपने कर्त्तव्य को पहचानेंगे और उसे पूर्ण करेंगे। तब आप धर्म तथा राजनीति के विषय में समझदार और स्वतन्त्र हो जाएँगे। तब आपको स्वार्थी पण्डे-पुजारी और पूँजीवादी एवं तथाकथित साम्यवादी, राजनीतिज्ञ, षड्यन्त्रकारी न तो धोखा दे सकेंगे और न ठग सकेंगे। क्या यह एक उदात्त उद्देश्य नहीं कि जिसके लिए प्रयत्न किया जाए ? आज अधिकांश मनुष्य न तो स्वतन्त्र हैं और न बुद्धिमान्। वे पतंगों के सामन है, जिनकी डोर या तो पण्डे-पुजारियों के या राजनीतिज्ञों के हाथों में होती है। विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा अन्य विषयों से अनभिज्ञ होने के कारण वे ठगे तथा मूर्ख बनाए जाते हैं। मानव जाति के कष्टों का आधा भाग अज्ञान के कारण ही है और इनका दूसरा आधा भाग अहंकार के कारण है। ज्ञान पूरी चरह उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितनी कि नैतिकता यानी आचार-सम्बन्धी विज्ञान। ये दोनों वस्तुतः अन्योन्याश्रित हैं। जैसा कि लेसिंग का कथन है, ‘‘ज्ञान का उद्देश्य है सत्य, और सत्य आत्मा की आवश्यकता है।’’ फारसी के कवि सादी ने ज़ोर देकर कहा है कि सभी को ज्ञान-प्राप्ति के लिए अथक प्रयत्न करना चाहिए- ज्ञान की साधना में तू फ़ौलाद की भाँति पिघल जा, तभी तू उसके साँचे में ढल सकेगा। ज्ञान पाने के लिए चाहे तुझे सारे संसार में भ्रमण करना पड़े, तो भी तू मत घबरा। यह तेरा कर्त्तव्य है।
ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने अनन्त संघर्ष में आपको अवश्यमेव नियमित रूप से तथा विधिपूर्वक प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रतिदिन अपने समय का एक निश्चित भाग आपको अध्ययन अथवा परीक्षण-प्रयोग में लगाना पड़ेगा। आप अपने शरीर को दिन में कई बार खुराक देते हैं; किन्तु अपने मस्तिष्क को भूखा मत रखिए। अपने पास एक दैनन्दिनी रखिए, जिसमें आप नई पुस्तकों के नाम अंकित करते रहिए। पुस्तक-विक्रेताओं से नई-पुरानी पुस्तकों के सूचीपात्र प्राप्त कीजिए। दूकानों पर सस्ती पुरानी पुस्तकों के लिए चक्कर लगाइए। अपनी एक स्वतन्त्र लाइब्रेरी बनाइए, चाहे वह कितनी ही छोटी हो। उन पुस्तकों पर गर्व कीजिए, जो आपके घर की शोभा बढ़ाती हैं। प्रत्येक पुस्तक को खरीदने के बाद, आप अपने मानसिक आकार में एक मिलीमीटर की वृद्धि करते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों से और अपने मित्रों से पुस्तकें माँगकर लाइए और पढ़िए और उन्हें समय पर लौटाना न भूलिए। जो भी पुस्तक आप पढ़ें, उसका सार और संक्षेप अपनी संचिका पर लिखते जाइए, अन्यथा आपका अध्ययन उस वर्षा के समान व्यर्थ होगा, जो ढालू छत पर होती है। समय-समय पर अपने लिखे सार-संक्षेप का पुनरावलोकन करके उसे अपनी स्मृति में नवीन बनाते रहिए। मेकाले के समान, अपने ज्ञान को तुरन्त ‘उपस्थित’ रखिए, आप जो कुछ जानते हैं, यथातथ्येन जानिए, जिस प्रकार आपको सही पता होता है कि आपके बैंक के खाते में कितना रुपया जमा है। अथवा एक गृहणी जानती है कि उसके भण्डार-घर में क्या कुछ है। कुछ वर्ष पहले ही अपने अध्ययन की योजना बना लीजिए। अपनी आय का एक निश्चित भाग पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ खरीदने के लिए अलग रखते जाइए, इसे आप ‘पुस्तक निधि’ कहिए, और इस पैसे को किसी भी अन्य खर्च के लिए मत निकलवाइए। इस प्रकार आपको पुस्तकों पर व्यय करना आसान प्रतीत होगा। विज्ञान तथा साहित्य सम्बन्धी संस्थाओं के सदस्य बन जाइए, उनको थोड़े-से चन्दे देने से मत घबराइए। एक छोटा-सा मण्डल बना लेना अच्छा है, जिसमें एक सदस्य नई पुस्तक को पढ़कर सुनाए और बाकी सब उसे सुनें, फिर वह उस पर एक निबन्ध लिखकर सुनाए, जिसमें उस पुस्तक के खूब उद्धरण दिए गए हैं। इस प्रकार का सहकारी अध्ययन आपके लिए आवश्यक है; क्योंकि अभाग्य से, आपके पास समय की बहुत कमी है। जीवन छोटा-सा है, ज्ञान-पिपासु के लिए जीवन और भी छोटा। यदि आपका जीवन अनन्त होता तो आप भले ही सौ वर्ष नक्षत्रविद्या के अध्ययन में, सौ वर्ष जीव-विज्ञान में, सौ वर्ष इतिहास के अध्ययन में, और सौ-वर्ष अन्यान्य विद्याओं के अध्ययन में लगा देते और तब तक अध्ययन करते चले जाते, जब तक कि अपने को भली-भाँति शिक्षित न मान लेते। किन्तु हमारा जीवन महीनों और वर्षों द्वारा मापा जाता है, शताब्दियों और सहस्त्राब्दियों से नहीं। बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व ही हम वृद्ध हो जाते हैं। इसीलिए अध्ययन करने में शीघ्रता कीजिए। प्रसिद्ध इतिहासकार जे.आर. ग्रीन ने लिखा है-‘‘मैं जानता हूँ लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, वे कहेंगे-‘वह पढ़ता-पढ़ता मर गया।’’ लोग आपके लिए भी यही कहें, तो अच्छा है। सम्भव है, इस लघु जीवन से विदा होकर पुनः आपको जन्म मिले और पुनः आपको अध्ययन का अवसर मिले।
मानसिक आत्म-संस्कार के मार्ग में दो विघ्न हैं-सबसे पहले आपको उन पर विजय प्राप्त करनी है-
बहुत-से स्त्री-पुरुष इतने धन-चिन्तक हैं कि वे कोई भी ऐसा कार्य गम्भीरता से हाथ में नहीं लेते, जिससे उन्हें धन का लाभ न हो। वे विश्वास रखते हैं-इस प्रकार का अध्ययन तथा मानसिक प्रयत्न मूर्खता है, जिसका परिणाम ‘धन का लाभ’ न हो। केवल धन के लाभ के लिए कठोर परिश्रम करो, उसके बाद खूब खेलो और आनन्द मनाओ। यह उन लोगों का जीवन-नियम होता है। वे बुद्धि का मूल्य यही मानते हैं कि वह भौतिक सम्पन्नता की कुँजी हो। वे लोग व्यक्तिगत मानसिक विकास को मूर्खतापूर्ण सनक मानते हैं। यह शोचनीय पदार्थवादी (Materialistic) मनोवृत्ति समाज के सभी वर्गो में गहरी जड़ जमाए हुए है। धनी और निर्धन, सभी को यह रोग लगा हुआ है। एक वृद्धा जो स्वयं उपार्जन के लिए काम करती थी, मुझसे अपने बेटे की शिकायत करते हुए कहने लगी, ‘‘वह अपना पैसा पुस्तकों पर बर्बाद करता रहता है। भला, उनका उसे क्या लाभ है ? वह तो एक बढ़ई है, कोई अध्यापक तो नहीं है।’’ ऐसे अगणित लोगों से मिलने का हमें मौका मिलता है, जिसका जीवन, उनके धन्धे और मनोरंजन की आँखमिचौनी में बीत जाता है। वे भले ही अपने व्यवसाय या धन्धे में सफल हुए हों-चाहे वह कानून हो या डाक्टरी, कला हो या कौशल-जब वे अपने रोज़गार से फुर्सत पाते हैं तो वे केवल मनोरंजन या खेल-तमाशे की ओर ही आकृष्ट होते हैं।
इस प्रकार के एकांगी को मेरा यह कहना है-ध्यान रखिए, कहीं आप छाया को पकड़कर तत्त्व को न छोड़ दें। ज्ञान ही जीवन का सार-तत्त्व है। आप भले ही अपने मस्तिष्क को धन के साँचे में ढाल दें; किन्तु यह समझ लीजिए की आप प्रकृति के इस वरदान का दुरुपयोग कर रहे हैं। बुद्धि का प्रयोग मुख्यतः जीवन के विकास और समाज की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग अपने सहनागरिकों के शोषण के लिए एक अस्त्र के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को एक धन कमाने की मशीन मानते हैं, उनमें और एक वेश्या में अन्तर ही क्या है ? हमारे पूँजीवादी समाज में इस प्रकार की वेश्यावृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है, और दुःख तो यह है कि इसे आप स्वाभाविक मानकर इसके आगे सिर झुका देते हैं। आप इस स्थिति के विरुद्ध न तो विद्रोह करते हैं और न इस पर आपको आश्चर्य ही होता है। प्रकृति ने आपको मस्तिष्क इसलिए दिया है कि आप जानें सोचें, समझें, समझाएँ, खोज करें, अनुसन्धान करें, आविष्कार करें, और उस सघन आनन्द का अनुभव करें, जो उन व्यक्तियों को प्राप्त होता है, जो प्रकृति के महान नियम का पालन करते हैं। जिज्ञासुओं को ज्ञान की उपलब्धि से जो आनन्द प्राप्त होता है, उसे शब्दों द्वारा वर्णन करना असंभव है। यदि आप अपने मस्तिष्क के सर्वतोमुखी विकास करने से मुँह मोडेंगे, तो आप अपने को अनन्त आनन्द से वंचित कर देगें। यह आनन्द उन सभी सुखों से श्रेष्ठ है, जिन्हें धन द्वारा खरीदा जा सके। इसलिए बुद्धि की दृष्टि से बौने रहकर जीने पर सन्तोष मत कीजिए। गधे की तरह भारीवाही जीवन को अधिकार है। अपने मस्तिष्क का अधिकतम विकास करके ही आप जीवन से श्रेष्टतम आनन्द को प्राप्त कर सकते हैं।
ज्ञान की प्राप्ति में दूसरा विघ्न है-अन्धविश्वास व रुढ़िवाद। इन्हीं के कारण लाखों-करोड़ों लोग बौद्धिक संस्कृति से वंचित रह जाते हैं। इन्हीं के कारण लोग अपने अज्ञान और मूढ़ता पर गर्व करते पाए जाते हैं। यह बात आपको विचित्र प्रतीत होगी; किन्तु है यह यथार्थ।
कुछ एक धार्मिक उपदेष्टाओं का कथन है कि मनुष्य-जीवन शरीर तथा आत्मा से बना है। किन्तु वे उपदेष्टा बुद्धि के विषय में मौन ही रहे। उनके अनुयायी संसार में शरीर को पुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं और आत्मा को ‘मृत्यु’ के उपरान्त जीवन’ के लिए सुरक्षित रखते हैं; किन्तु ‘मन’ की सर्वथा उपेक्षा कर देते हैं। इहलोक और परलोक में मानव-कल्याण के हेतु-शरीर के लिए भोजन और आत्मा के लिए सद्गुण-ये अनिवार्यतः आवश्यक माने जाते हैं। किन्तु ज्ञान तथा शिक्षा के बारे में कुछ कहना अनावश्यक समझा जाता है। इसी तरह ईसामसीह ने भूखे को भोजन देने, रोगी की चिकित्सा करने, पापी को पुण्यात्मा बनाने का तो उपदेश दिया; किन्तु उन्होंने कभी भी यह उपदेश न दिया कि अज्ञानी को ज्ञान प्रदान करो, या वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि करो। वे स्वयं भी सुशिक्षित व्यक्ति नहीं थे और बुद्धि-सम्बन्धी प्रयत्न उनकी सीमा से बाहर थे। गौतम बुद्ध ने भी सदाचार पर बल दिया, ध्यान करने और भिक्षु बनने का उपदेश दिया; किन्तु उन्होंने इतिहास, विज्ञान, कला तथा साहित्य के अध्ययन पर कभी ज़ोर नहीं दिया। सन्त एम्ब्रोस ने विज्ञान के अध्ययन की निन्दा की और लिखा, ‘‘प्रकृति और पृथ्वी की स्थिति आदि पर विचार, चर्चा या वाद-विवाद हमारे पारलौकिक जीवन में कुछ भी सहायता प्रदान नहीं करता।’’ सन्त बासिल ने बहुत स्पष्ट रूप में और मूर्खतापूर्वक कहा- ‘‘हमारे लिए यह पृथ्वी गोल है, लम्बी है या सपाट है।’’ कार्लायल ने भी ईसाई परम्परा का ही अनुसरण किया है, जबकि उसने कहा,‘‘मैं केवल दो मनुष्यों का सम्मान करता हूँ (तीसरे का नहीं), एक तो शारीरिक परिश्रम करने वाले का और दूसरे धार्मिक उपदेशक का।’’
कार्लायल ने वैज्ञानिक को, विद्वान को और कलाकार को सम्मान की सूची में शामिल करने से भुला दिया। यूनान के सनकी भी शिक्षा, बौद्धिक साधना की निन्दा करते रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि केवल सद्गुण (सदाचार) ही जीवन की श्रेष्ठता है। इस प्रकार के अपूर्ण आदर्श ने ही असंख्य ईमानदार स्त्री-पुरुषों को बुद्धि की साधना से-ज्ञान के उपार्जन से वंचित रखा है, क्योंकि इन्हें अनावश्यक और व्यर्थ समझते रहे हैं। आप अपने मस्तिष्क को, जीवन के विषय में इस प्रकार के अपूर्ण सूत्रों का दास मत बनने दीजिए। ये सिद्धान्त थोथे हैं-सारहीन हैं, इनसे सर्वोत्तम प्रकार के स्त्री-पुरुष भी ‘सदाचारी और पवित्र पशु’ बना दिए जाते हैं। अज्ञान जंगलीपन है, वहशीपन है, मानव जीवन की स्वाभाविक विशेषता ‘ज्ञान’ है।
अविवेक, कामुकता और अंधविश्वास से छुटकारा पाकर आप अपने को परिश्रमपूर्वक और ईमानदारी से मानसिक आत्म-संस्कार में-मस्तिष्क द्वारा ज्ञानार्जन में लगाइए। इसका क्षेत्र बहुत विशाल और वित्तृत है। पहले-पहल आपकी दशा एक बालक के समान होगी, जो अकस्मात् अपने को उष्णकटिबन्ध के किसी महा-उद्यान में पाता है, जहाँ अनेक प्रकार के सुस्वादु फलों को देखकर उसकी दृष्टि चकाचौंध रह जाती है, उसके मुँह में उन फलों को देखकर पानी भर आता है-कहीं आम हैं, कहीं लीची, कहीं अमरूद हैं, कहीं पपीते, कहीं लुकाठ हैं, कहीं अँगूर। ज्ञान के फल तो इनसे भी अधिक सरस और सुस्वादु हैं।
अब हमें उन विभिन्न विषयों पर विचार करना है, जो आपको अवश्य पढ़ने चाहिए, जहाँ तब कि आपके साधन, आपकी सामर्थ्य और आपके अवसर आपको इजाज़त दें।
ज्ञान तथा मानसिक आत्म-संस्कार से आप पर अवर्णनीय वरदानों की वर्षा होगी। इससे आप धर्म और राजनीति के बारे में अन्धविश्वासों और रुढ़ियों के दास नहीं रहेंगे। तब आप अपने कर्त्तव्य को पहचानेंगे और उसे पूर्ण करेंगे। तब आप धर्म तथा राजनीति के विषय में समझदार और स्वतन्त्र हो जाएँगे। तब आपको स्वार्थी पण्डे-पुजारी और पूँजीवादी एवं तथाकथित साम्यवादी, राजनीतिज्ञ, षड्यन्त्रकारी न तो धोखा दे सकेंगे और न ठग सकेंगे। क्या यह एक उदात्त उद्देश्य नहीं कि जिसके लिए प्रयत्न किया जाए ? आज अधिकांश मनुष्य न तो स्वतन्त्र हैं और न बुद्धिमान्। वे पतंगों के सामन है, जिनकी डोर या तो पण्डे-पुजारियों के या राजनीतिज्ञों के हाथों में होती है। विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा अन्य विषयों से अनभिज्ञ होने के कारण वे ठगे तथा मूर्ख बनाए जाते हैं। मानव जाति के कष्टों का आधा भाग अज्ञान के कारण ही है और इनका दूसरा आधा भाग अहंकार के कारण है। ज्ञान पूरी चरह उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितनी कि नैतिकता यानी आचार-सम्बन्धी विज्ञान। ये दोनों वस्तुतः अन्योन्याश्रित हैं। जैसा कि लेसिंग का कथन है, ‘‘ज्ञान का उद्देश्य है सत्य, और सत्य आत्मा की आवश्यकता है।’’ फारसी के कवि सादी ने ज़ोर देकर कहा है कि सभी को ज्ञान-प्राप्ति के लिए अथक प्रयत्न करना चाहिए- ज्ञान की साधना में तू फ़ौलाद की भाँति पिघल जा, तभी तू उसके साँचे में ढल सकेगा। ज्ञान पाने के लिए चाहे तुझे सारे संसार में भ्रमण करना पड़े, तो भी तू मत घबरा। यह तेरा कर्त्तव्य है।
ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने अनन्त संघर्ष में आपको अवश्यमेव नियमित रूप से तथा विधिपूर्वक प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रतिदिन अपने समय का एक निश्चित भाग आपको अध्ययन अथवा परीक्षण-प्रयोग में लगाना पड़ेगा। आप अपने शरीर को दिन में कई बार खुराक देते हैं; किन्तु अपने मस्तिष्क को भूखा मत रखिए। अपने पास एक दैनन्दिनी रखिए, जिसमें आप नई पुस्तकों के नाम अंकित करते रहिए। पुस्तक-विक्रेताओं से नई-पुरानी पुस्तकों के सूचीपात्र प्राप्त कीजिए। दूकानों पर सस्ती पुरानी पुस्तकों के लिए चक्कर लगाइए। अपनी एक स्वतन्त्र लाइब्रेरी बनाइए, चाहे वह कितनी ही छोटी हो। उन पुस्तकों पर गर्व कीजिए, जो आपके घर की शोभा बढ़ाती हैं। प्रत्येक पुस्तक को खरीदने के बाद, आप अपने मानसिक आकार में एक मिलीमीटर की वृद्धि करते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों से और अपने मित्रों से पुस्तकें माँगकर लाइए और पढ़िए और उन्हें समय पर लौटाना न भूलिए। जो भी पुस्तक आप पढ़ें, उसका सार और संक्षेप अपनी संचिका पर लिखते जाइए, अन्यथा आपका अध्ययन उस वर्षा के समान व्यर्थ होगा, जो ढालू छत पर होती है। समय-समय पर अपने लिखे सार-संक्षेप का पुनरावलोकन करके उसे अपनी स्मृति में नवीन बनाते रहिए। मेकाले के समान, अपने ज्ञान को तुरन्त ‘उपस्थित’ रखिए, आप जो कुछ जानते हैं, यथातथ्येन जानिए, जिस प्रकार आपको सही पता होता है कि आपके बैंक के खाते में कितना रुपया जमा है। अथवा एक गृहणी जानती है कि उसके भण्डार-घर में क्या कुछ है। कुछ वर्ष पहले ही अपने अध्ययन की योजना बना लीजिए। अपनी आय का एक निश्चित भाग पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ खरीदने के लिए अलग रखते जाइए, इसे आप ‘पुस्तक निधि’ कहिए, और इस पैसे को किसी भी अन्य खर्च के लिए मत निकलवाइए। इस प्रकार आपको पुस्तकों पर व्यय करना आसान प्रतीत होगा। विज्ञान तथा साहित्य सम्बन्धी संस्थाओं के सदस्य बन जाइए, उनको थोड़े-से चन्दे देने से मत घबराइए। एक छोटा-सा मण्डल बना लेना अच्छा है, जिसमें एक सदस्य नई पुस्तक को पढ़कर सुनाए और बाकी सब उसे सुनें, फिर वह उस पर एक निबन्ध लिखकर सुनाए, जिसमें उस पुस्तक के खूब उद्धरण दिए गए हैं। इस प्रकार का सहकारी अध्ययन आपके लिए आवश्यक है; क्योंकि अभाग्य से, आपके पास समय की बहुत कमी है। जीवन छोटा-सा है, ज्ञान-पिपासु के लिए जीवन और भी छोटा। यदि आपका जीवन अनन्त होता तो आप भले ही सौ वर्ष नक्षत्रविद्या के अध्ययन में, सौ वर्ष जीव-विज्ञान में, सौ वर्ष इतिहास के अध्ययन में, और सौ-वर्ष अन्यान्य विद्याओं के अध्ययन में लगा देते और तब तक अध्ययन करते चले जाते, जब तक कि अपने को भली-भाँति शिक्षित न मान लेते। किन्तु हमारा जीवन महीनों और वर्षों द्वारा मापा जाता है, शताब्दियों और सहस्त्राब्दियों से नहीं। बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व ही हम वृद्ध हो जाते हैं। इसीलिए अध्ययन करने में शीघ्रता कीजिए। प्रसिद्ध इतिहासकार जे.आर. ग्रीन ने लिखा है-‘‘मैं जानता हूँ लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, वे कहेंगे-‘वह पढ़ता-पढ़ता मर गया।’’ लोग आपके लिए भी यही कहें, तो अच्छा है। सम्भव है, इस लघु जीवन से विदा होकर पुनः आपको जन्म मिले और पुनः आपको अध्ययन का अवसर मिले।
मानसिक आत्म-संस्कार के मार्ग में दो विघ्न हैं-सबसे पहले आपको उन पर विजय प्राप्त करनी है-
बहुत-से स्त्री-पुरुष इतने धन-चिन्तक हैं कि वे कोई भी ऐसा कार्य गम्भीरता से हाथ में नहीं लेते, जिससे उन्हें धन का लाभ न हो। वे विश्वास रखते हैं-इस प्रकार का अध्ययन तथा मानसिक प्रयत्न मूर्खता है, जिसका परिणाम ‘धन का लाभ’ न हो। केवल धन के लाभ के लिए कठोर परिश्रम करो, उसके बाद खूब खेलो और आनन्द मनाओ। यह उन लोगों का जीवन-नियम होता है। वे बुद्धि का मूल्य यही मानते हैं कि वह भौतिक सम्पन्नता की कुँजी हो। वे लोग व्यक्तिगत मानसिक विकास को मूर्खतापूर्ण सनक मानते हैं। यह शोचनीय पदार्थवादी (Materialistic) मनोवृत्ति समाज के सभी वर्गो में गहरी जड़ जमाए हुए है। धनी और निर्धन, सभी को यह रोग लगा हुआ है। एक वृद्धा जो स्वयं उपार्जन के लिए काम करती थी, मुझसे अपने बेटे की शिकायत करते हुए कहने लगी, ‘‘वह अपना पैसा पुस्तकों पर बर्बाद करता रहता है। भला, उनका उसे क्या लाभ है ? वह तो एक बढ़ई है, कोई अध्यापक तो नहीं है।’’ ऐसे अगणित लोगों से मिलने का हमें मौका मिलता है, जिसका जीवन, उनके धन्धे और मनोरंजन की आँखमिचौनी में बीत जाता है। वे भले ही अपने व्यवसाय या धन्धे में सफल हुए हों-चाहे वह कानून हो या डाक्टरी, कला हो या कौशल-जब वे अपने रोज़गार से फुर्सत पाते हैं तो वे केवल मनोरंजन या खेल-तमाशे की ओर ही आकृष्ट होते हैं।
इस प्रकार के एकांगी को मेरा यह कहना है-ध्यान रखिए, कहीं आप छाया को पकड़कर तत्त्व को न छोड़ दें। ज्ञान ही जीवन का सार-तत्त्व है। आप भले ही अपने मस्तिष्क को धन के साँचे में ढाल दें; किन्तु यह समझ लीजिए की आप प्रकृति के इस वरदान का दुरुपयोग कर रहे हैं। बुद्धि का प्रयोग मुख्यतः जीवन के विकास और समाज की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग अपने सहनागरिकों के शोषण के लिए एक अस्त्र के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को एक धन कमाने की मशीन मानते हैं, उनमें और एक वेश्या में अन्तर ही क्या है ? हमारे पूँजीवादी समाज में इस प्रकार की वेश्यावृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है, और दुःख तो यह है कि इसे आप स्वाभाविक मानकर इसके आगे सिर झुका देते हैं। आप इस स्थिति के विरुद्ध न तो विद्रोह करते हैं और न इस पर आपको आश्चर्य ही होता है। प्रकृति ने आपको मस्तिष्क इसलिए दिया है कि आप जानें सोचें, समझें, समझाएँ, खोज करें, अनुसन्धान करें, आविष्कार करें, और उस सघन आनन्द का अनुभव करें, जो उन व्यक्तियों को प्राप्त होता है, जो प्रकृति के महान नियम का पालन करते हैं। जिज्ञासुओं को ज्ञान की उपलब्धि से जो आनन्द प्राप्त होता है, उसे शब्दों द्वारा वर्णन करना असंभव है। यदि आप अपने मस्तिष्क के सर्वतोमुखी विकास करने से मुँह मोडेंगे, तो आप अपने को अनन्त आनन्द से वंचित कर देगें। यह आनन्द उन सभी सुखों से श्रेष्ठ है, जिन्हें धन द्वारा खरीदा जा सके। इसलिए बुद्धि की दृष्टि से बौने रहकर जीने पर सन्तोष मत कीजिए। गधे की तरह भारीवाही जीवन को अधिकार है। अपने मस्तिष्क का अधिकतम विकास करके ही आप जीवन से श्रेष्टतम आनन्द को प्राप्त कर सकते हैं।
ज्ञान की प्राप्ति में दूसरा विघ्न है-अन्धविश्वास व रुढ़िवाद। इन्हीं के कारण लाखों-करोड़ों लोग बौद्धिक संस्कृति से वंचित रह जाते हैं। इन्हीं के कारण लोग अपने अज्ञान और मूढ़ता पर गर्व करते पाए जाते हैं। यह बात आपको विचित्र प्रतीत होगी; किन्तु है यह यथार्थ।
कुछ एक धार्मिक उपदेष्टाओं का कथन है कि मनुष्य-जीवन शरीर तथा आत्मा से बना है। किन्तु वे उपदेष्टा बुद्धि के विषय में मौन ही रहे। उनके अनुयायी संसार में शरीर को पुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं और आत्मा को ‘मृत्यु’ के उपरान्त जीवन’ के लिए सुरक्षित रखते हैं; किन्तु ‘मन’ की सर्वथा उपेक्षा कर देते हैं। इहलोक और परलोक में मानव-कल्याण के हेतु-शरीर के लिए भोजन और आत्मा के लिए सद्गुण-ये अनिवार्यतः आवश्यक माने जाते हैं। किन्तु ज्ञान तथा शिक्षा के बारे में कुछ कहना अनावश्यक समझा जाता है। इसी तरह ईसामसीह ने भूखे को भोजन देने, रोगी की चिकित्सा करने, पापी को पुण्यात्मा बनाने का तो उपदेश दिया; किन्तु उन्होंने कभी भी यह उपदेश न दिया कि अज्ञानी को ज्ञान प्रदान करो, या वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि करो। वे स्वयं भी सुशिक्षित व्यक्ति नहीं थे और बुद्धि-सम्बन्धी प्रयत्न उनकी सीमा से बाहर थे। गौतम बुद्ध ने भी सदाचार पर बल दिया, ध्यान करने और भिक्षु बनने का उपदेश दिया; किन्तु उन्होंने इतिहास, विज्ञान, कला तथा साहित्य के अध्ययन पर कभी ज़ोर नहीं दिया। सन्त एम्ब्रोस ने विज्ञान के अध्ययन की निन्दा की और लिखा, ‘‘प्रकृति और पृथ्वी की स्थिति आदि पर विचार, चर्चा या वाद-विवाद हमारे पारलौकिक जीवन में कुछ भी सहायता प्रदान नहीं करता।’’ सन्त बासिल ने बहुत स्पष्ट रूप में और मूर्खतापूर्वक कहा- ‘‘हमारे लिए यह पृथ्वी गोल है, लम्बी है या सपाट है।’’ कार्लायल ने भी ईसाई परम्परा का ही अनुसरण किया है, जबकि उसने कहा,‘‘मैं केवल दो मनुष्यों का सम्मान करता हूँ (तीसरे का नहीं), एक तो शारीरिक परिश्रम करने वाले का और दूसरे धार्मिक उपदेशक का।’’
कार्लायल ने वैज्ञानिक को, विद्वान को और कलाकार को सम्मान की सूची में शामिल करने से भुला दिया। यूनान के सनकी भी शिक्षा, बौद्धिक साधना की निन्दा करते रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि केवल सद्गुण (सदाचार) ही जीवन की श्रेष्ठता है। इस प्रकार के अपूर्ण आदर्श ने ही असंख्य ईमानदार स्त्री-पुरुषों को बुद्धि की साधना से-ज्ञान के उपार्जन से वंचित रखा है, क्योंकि इन्हें अनावश्यक और व्यर्थ समझते रहे हैं। आप अपने मस्तिष्क को, जीवन के विषय में इस प्रकार के अपूर्ण सूत्रों का दास मत बनने दीजिए। ये सिद्धान्त थोथे हैं-सारहीन हैं, इनसे सर्वोत्तम प्रकार के स्त्री-पुरुष भी ‘सदाचारी और पवित्र पशु’ बना दिए जाते हैं। अज्ञान जंगलीपन है, वहशीपन है, मानव जीवन की स्वाभाविक विशेषता ‘ज्ञान’ है।
अविवेक, कामुकता और अंधविश्वास से छुटकारा पाकर आप अपने को परिश्रमपूर्वक और ईमानदारी से मानसिक आत्म-संस्कार में-मस्तिष्क द्वारा ज्ञानार्जन में लगाइए। इसका क्षेत्र बहुत विशाल और वित्तृत है। पहले-पहल आपकी दशा एक बालक के समान होगी, जो अकस्मात् अपने को उष्णकटिबन्ध के किसी महा-उद्यान में पाता है, जहाँ अनेक प्रकार के सुस्वादु फलों को देखकर उसकी दृष्टि चकाचौंध रह जाती है, उसके मुँह में उन फलों को देखकर पानी भर आता है-कहीं आम हैं, कहीं लीची, कहीं अमरूद हैं, कहीं पपीते, कहीं लुकाठ हैं, कहीं अँगूर। ज्ञान के फल तो इनसे भी अधिक सरस और सुस्वादु हैं।
अब हमें उन विभिन्न विषयों पर विचार करना है, जो आपको अवश्य पढ़ने चाहिए, जहाँ तब कि आपके साधन, आपकी सामर्थ्य और आपके अवसर आपको इजाज़त दें।
(2)
विज्ञान का अध्ययन
प्रकृति-विज्ञान का अध्ययन, शिक्षा का एक अनिवार्य अंग है। आपका विज्ञान का अध्ययन हरबर्ट स्पेंसर या डारविन के समान एकांगी नहीं होना चाहिए हरबर्ट स्पेंसर का विचार था कि प्राकृतिक विज्ञान ही अध्ययन के लिए एकमात्र बहुमूल्य यानी महत्त्वपूर्ण विषय है और डारविन ने अपनी अति विज्ञान-भक्ति के कारण, कला से प्राप्त होने वाले आनन्द को प्रायः खो दिया था। आप विज्ञान को उसका उचित स्थान दें, भले ही आप आवश्यक से कुछ अधिक स्थान उसे दें; क्योंकि वर्तमान में-साहित्य, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र की तुलमा में विज्ञान की प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है।
हो सकता है, आप यह सोचें कि विज्ञान एक शुष्क, कठिन और अनाकर्षक विषय है, यह पारिभाषिक शब्दावली तथा कठिनतर सूत्रों से पूर्ण है। लेकिन आपके लिए यह आवश्यक नहीं कि प्राकृतिक विज्ञान की सभी शाखाओं के आप आचार्य बन जाएँ-यह काम तो प्राकृतिक विज्ञान की प्रत्येक शाखा के विशेषज्ञों का है। वास्तव में, जिस दिन से आपका जन्म हुआ है, उसी दिन से सामान्यतः आपका विज्ञान से सम्बन्ध हो गया है। इस प्रशंसा पर सम्भव है आपको आश्चर्य होगा; किन्तु आपको यह जान लेना चाहिए कि विज्ञान का अर्थ है-प्रकृति के असाधारण तथ्यों का निरीक्षण, सीमित स्थितियों में परीक्षण, वर्गीकरण और प्रमाणीकरण परिणामन, अनुमान, नियमों की रचना और तर्क के लिए अनुमान, अनुसन्धान और आविष्कार, जीवन के व्यावहारिक कार्यों में ज्ञान का उपयोग-इत्यादि है। जब आप एक बालक थे-आप पक्षियों तथा कीट-पतंगों की आदतों का निरीक्षण किया करते थे और उनके बारे में अपने कुछ निर्णयों पर पहुँचे थे, उस समय आप एक नौसिखिया वैज्ञानिक की भाँति आचरण कर रहे थे।
विज्ञान आपको यह बताता है कि आप अपनी आँखों और कानों को खुला रखें। आप जिन तथ्यों को प्रत्यक्ष ग्रहण करेंगे-आपका सचेतन मन और प्रशिक्षित मस्तिष्क उन तथ्यों के प्रभावों और महत्त्वों को विस्तार से समझेगा। प्रकृति के समस्त आश्चर्यों को अध्ययन विज्ञान में आ जाता है। प्रकृति में मानव भी सम्मिलित है न ! आपकी अन्तर्जात कौतूहल-वृत्ति आपको प्रोत्साहित करती है कि आप अपने इर्द-गिर्द के पदार्थों और होने वाली चेष्टाओं-घटनाओं का निरीक्षण करें। आप सूर्य को और सितारों को, पौधों, को और पशुओं को देखते हैं। आपकी कौतूल-वृत्ति और अभिरुचि जागृत हो जाती है। इस ब्रह्म सृष्टि के ‘क्या, क्यों और कैसे’ को आप जानना चाहते हैं। अतएव आप वैज्ञानिक हुए बिना रह ही नहीं सकते। जैसा कि टी-एच. हक्सले ने कहा है-‘‘प्रशिक्षण और सुगठित समझ का नाम ही विज्ञान है।’’ इस प्राकृतिक कौतूहल-वृत्ति को कुणठित न होने दीजिए; किन्तु यदि आप इसे वैज्ञानिक अध्ययन या खोज का अवसर नहीं देंगे, तो यह अवश्य मेव कुण्ठित हो आएगी। जब आप प्रकृति के आश्चर्यों पर चकित या आकर्षित होना बन्द कर देंगे, तब आप बौद्धिक दृष्टि से निष्क्रिय हो जाएँगे, बस आप मुर्दा के समान हो जाएँगे। नियमित प्रकृति-अध्ययन-दैनन्दिनी अपने पास रखना, एक अत्युत्तम योजना है। उस दैनन्दिनी में आप उन प्राकृतिक आश्चरों को लिख सकते हैं, जिनका आपने निरीक्षण किया हो। एक सुन्दर सूर्यास्त, एक दोहरा इन्द्रधनुष, जंगली फूलों की एक क्यारी, पक्षियों की उड़ान, उल्लू की घूँ-घूँ, चींटियों का पर्वत, उड़ती मछलियाँ, वनस्पति-सुषमा और प्रकृति के अगणित दृश्यों तथा ध्वनियों को आपकी डायरी में स्थान मिल जाएगा। इस प्रकार अपने बुद्धिपूर्ण निरीक्षण का ऐसा विकास कर सकेंगे जो द्रुत हो। यह डायरी आपकी इस बात में भी सहायता करेगी कि आप अपने अन्तर्मन में-मन की आँखों से अतीत के उन विचित्र दृश्यों को एकान्त में देखने का आनन्द प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त विज्ञान आपको अंधविश्वासों से बचाएगा। यह सबसे बड़ा वरदान है, जो विज्ञान के साधकों को इससे प्राप्त होता है। आदिम मानव अंधविश्वासों के पालने में पला था; क्योंकि वह सभी प्राकृतिक आश्चर्यों का अपने से सम्बन्ध मानने के लिए तथा इनका कारण देवी, देवताओं, दैत्यों अप्सराओं आदि को मानने के लिए विवश था। सभ्यता के शैशव-काल में, मिथ्या विश्वास मानवजाति का व्यापक शत्रु था। किंतु विज्ञान और केवल विज्ञान ही मानव के मस्तिष्क को स्वतन्त्रता और स्वाधीनता प्रदान कर सकता है, वह मानव-मस्तिष्क को मिथ्या विश्वास के सब स्वरूपों और छलनामय रूपों से उसका उद्धार कर सकता है।
मिथ्या विश्वास का अर्थ है-जिसकी कोई सत्ता नहीं उसका अस्तित्व स्वीकार करना। यह सहस्त्र रूपों में मानवता को दासता के बन्धन में जकड़े हुए है। मानवजाति के इतिहास में, मिथ्या विश्वास ने क्रूर शोषण और निन्दनीय अत्याचारों के कई अध्याय बनाए हैं। प्रत्येक प्रकार का असत्य भयंकर होता है। मिथ्या विश्वास तो विशेषतया मुसीबतें ढानेवाला, चिरस्थाई और विनाशकारक असत्य है, जिसका भण्डाफोड़ केवल विज्ञान ही कर सकता है और विज्ञान ही इसे नष्ट कर सकता है। महान रोमन कवि-दार्शनिक लुक्रेशियस ने एक गीत में गाया था-‘‘मिथ्या विश्वास को पैरों के नीचे रखकर कुचल दो...मन का यह भयावह अंधकार अवश्य ही नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन इसे सूर्य की किरणों से नहीं, दिन की चमकती धूप से नहीं, बल्कि प्रकृति के सत्यों और नियमों से इसे नष्ट किया जा सकता है।
हो सकता है, आप यह सोचें कि विज्ञान एक शुष्क, कठिन और अनाकर्षक विषय है, यह पारिभाषिक शब्दावली तथा कठिनतर सूत्रों से पूर्ण है। लेकिन आपके लिए यह आवश्यक नहीं कि प्राकृतिक विज्ञान की सभी शाखाओं के आप आचार्य बन जाएँ-यह काम तो प्राकृतिक विज्ञान की प्रत्येक शाखा के विशेषज्ञों का है। वास्तव में, जिस दिन से आपका जन्म हुआ है, उसी दिन से सामान्यतः आपका विज्ञान से सम्बन्ध हो गया है। इस प्रशंसा पर सम्भव है आपको आश्चर्य होगा; किन्तु आपको यह जान लेना चाहिए कि विज्ञान का अर्थ है-प्रकृति के असाधारण तथ्यों का निरीक्षण, सीमित स्थितियों में परीक्षण, वर्गीकरण और प्रमाणीकरण परिणामन, अनुमान, नियमों की रचना और तर्क के लिए अनुमान, अनुसन्धान और आविष्कार, जीवन के व्यावहारिक कार्यों में ज्ञान का उपयोग-इत्यादि है। जब आप एक बालक थे-आप पक्षियों तथा कीट-पतंगों की आदतों का निरीक्षण किया करते थे और उनके बारे में अपने कुछ निर्णयों पर पहुँचे थे, उस समय आप एक नौसिखिया वैज्ञानिक की भाँति आचरण कर रहे थे।
विज्ञान आपको यह बताता है कि आप अपनी आँखों और कानों को खुला रखें। आप जिन तथ्यों को प्रत्यक्ष ग्रहण करेंगे-आपका सचेतन मन और प्रशिक्षित मस्तिष्क उन तथ्यों के प्रभावों और महत्त्वों को विस्तार से समझेगा। प्रकृति के समस्त आश्चर्यों को अध्ययन विज्ञान में आ जाता है। प्रकृति में मानव भी सम्मिलित है न ! आपकी अन्तर्जात कौतूहल-वृत्ति आपको प्रोत्साहित करती है कि आप अपने इर्द-गिर्द के पदार्थों और होने वाली चेष्टाओं-घटनाओं का निरीक्षण करें। आप सूर्य को और सितारों को, पौधों, को और पशुओं को देखते हैं। आपकी कौतूल-वृत्ति और अभिरुचि जागृत हो जाती है। इस ब्रह्म सृष्टि के ‘क्या, क्यों और कैसे’ को आप जानना चाहते हैं। अतएव आप वैज्ञानिक हुए बिना रह ही नहीं सकते। जैसा कि टी-एच. हक्सले ने कहा है-‘‘प्रशिक्षण और सुगठित समझ का नाम ही विज्ञान है।’’ इस प्राकृतिक कौतूहल-वृत्ति को कुणठित न होने दीजिए; किन्तु यदि आप इसे वैज्ञानिक अध्ययन या खोज का अवसर नहीं देंगे, तो यह अवश्य मेव कुण्ठित हो आएगी। जब आप प्रकृति के आश्चर्यों पर चकित या आकर्षित होना बन्द कर देंगे, तब आप बौद्धिक दृष्टि से निष्क्रिय हो जाएँगे, बस आप मुर्दा के समान हो जाएँगे। नियमित प्रकृति-अध्ययन-दैनन्दिनी अपने पास रखना, एक अत्युत्तम योजना है। उस दैनन्दिनी में आप उन प्राकृतिक आश्चरों को लिख सकते हैं, जिनका आपने निरीक्षण किया हो। एक सुन्दर सूर्यास्त, एक दोहरा इन्द्रधनुष, जंगली फूलों की एक क्यारी, पक्षियों की उड़ान, उल्लू की घूँ-घूँ, चींटियों का पर्वत, उड़ती मछलियाँ, वनस्पति-सुषमा और प्रकृति के अगणित दृश्यों तथा ध्वनियों को आपकी डायरी में स्थान मिल जाएगा। इस प्रकार अपने बुद्धिपूर्ण निरीक्षण का ऐसा विकास कर सकेंगे जो द्रुत हो। यह डायरी आपकी इस बात में भी सहायता करेगी कि आप अपने अन्तर्मन में-मन की आँखों से अतीत के उन विचित्र दृश्यों को एकान्त में देखने का आनन्द प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त विज्ञान आपको अंधविश्वासों से बचाएगा। यह सबसे बड़ा वरदान है, जो विज्ञान के साधकों को इससे प्राप्त होता है। आदिम मानव अंधविश्वासों के पालने में पला था; क्योंकि वह सभी प्राकृतिक आश्चर्यों का अपने से सम्बन्ध मानने के लिए तथा इनका कारण देवी, देवताओं, दैत्यों अप्सराओं आदि को मानने के लिए विवश था। सभ्यता के शैशव-काल में, मिथ्या विश्वास मानवजाति का व्यापक शत्रु था। किंतु विज्ञान और केवल विज्ञान ही मानव के मस्तिष्क को स्वतन्त्रता और स्वाधीनता प्रदान कर सकता है, वह मानव-मस्तिष्क को मिथ्या विश्वास के सब स्वरूपों और छलनामय रूपों से उसका उद्धार कर सकता है।
मिथ्या विश्वास का अर्थ है-जिसकी कोई सत्ता नहीं उसका अस्तित्व स्वीकार करना। यह सहस्त्र रूपों में मानवता को दासता के बन्धन में जकड़े हुए है। मानवजाति के इतिहास में, मिथ्या विश्वास ने क्रूर शोषण और निन्दनीय अत्याचारों के कई अध्याय बनाए हैं। प्रत्येक प्रकार का असत्य भयंकर होता है। मिथ्या विश्वास तो विशेषतया मुसीबतें ढानेवाला, चिरस्थाई और विनाशकारक असत्य है, जिसका भण्डाफोड़ केवल विज्ञान ही कर सकता है और विज्ञान ही इसे नष्ट कर सकता है। महान रोमन कवि-दार्शनिक लुक्रेशियस ने एक गीत में गाया था-‘‘मिथ्या विश्वास को पैरों के नीचे रखकर कुचल दो...मन का यह भयावह अंधकार अवश्य ही नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन इसे सूर्य की किरणों से नहीं, दिन की चमकती धूप से नहीं, बल्कि प्रकृति के सत्यों और नियमों से इसे नष्ट किया जा सकता है।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book